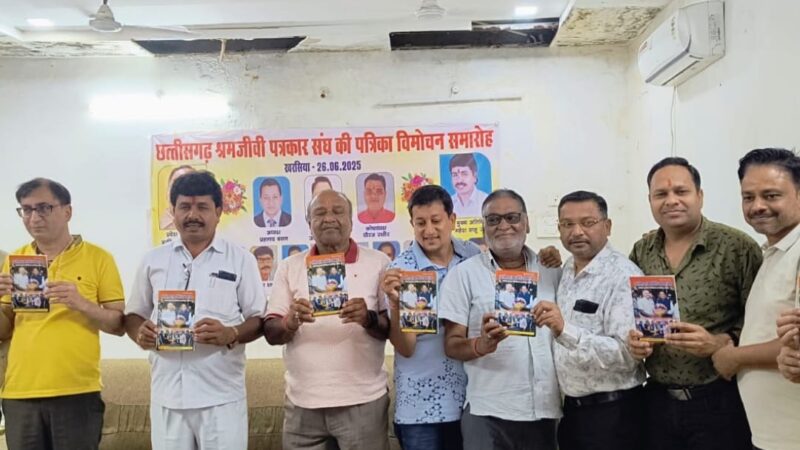सोशल मीडिया के अनसोशल नशे में कहीं आप भी तो नहीं फंसते जा रहे हैं…. जानिए कैसे

दिल्ली। दुनियाभर में सबसे अधिक आबादी वाले देशों की फेहरिस्त में भारत नंबर 2 पर है, लेकिन सोशल मीडिया के मामले में सबसे आगे है. अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के ही अकेले यहां पर 40 करोड़ अकाउंट हैं, वहीं वाट्सऐप के तो तकरीबन 53 करोड़ यूजर हैं.
बात नब्बे के दशक के शुरुआत की है, जब लेखक को भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी से इंटरनेट और सर्च इंजन (Internet And Search Engine) जैसी किसी चीज़ के बारे में पता चला. इसका इस्तेमाल विदेशों में वहां की पुलिस कर रही थी, जिससे पुलिस को कई तरीके से मदद मिल रही थी. ये दिलचस्प जानकारी थी और साथ ही उन दिनों इसे दिल्ली पुलिस (Delhi Police) भी इस्तेमाल करने पर विचार कर रही थी. तभी पता चला कि ये कोई ऐसी तकनीक है, जिसमें कंप्यूटर के एक क्लिक से ज्ञान का भंडार खुल जाता है. जो चाहो जानकारी झट से पा लो और फटाफट किसी को भी टाइप करके भेज दो.
सूचना (Information Technology) लेने देने के लिए तब तक की सबसे आधुनिक तकनीक मॉडेम थी जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के नेटवर्क के ज़रिए ही होता था. इसके अलावा , चलते फिरते कहीं भी संदेश पाने के लिए पेजर तक चुनिंदा पेशेवर लोगों की पहुंच हो चुकी थी. इससे कुछ साल पहले ही यानि 80 के दशक में रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर और फैक्स का आगमन भारत में हो चुका था, ये भारत में सूचना क्रांति से कम नहीं था. लेकिन ऐसे में इंटरनेट तो एक कदम क्या, कितने ही कदम आगे की चीज़ थी
थोड़े बहुत इल्म के साथ इस बारे में लेखक ने बतौर रिपोर्टर एक खबर लिखी, जो अखबार में प्रकाशित हुई. लिखने से लेकर, इसके छपने और छपकर घरों तक पहुंच जाने की प्रक्रिया में जिस-जिस की नज़र से ये जानकारी गुजरी, किसी को भी इस सच्चाई पर आसानी से यकीन नहीं हो रहा था कि ‘इंटरनेट’ और ‘सर्च इंजन’ जैसी कोई बला हो सकती है. वैसे भी उस ज़माने की जनता को इसका यकीं होता भी कैसे जब उसे घर में लैंड लाइन फोन लगवाने के लिए सालों इंतज़ार करने की आदत पड़ी हुई हो. तब फोन तो बहुत बड़े अधिकारियों या मंत्रियों को भी आसानी से नहीं मिलते थे.
तब किसने सोचा था कि जिंदगी को रफ्तार देने वाले ‘इंटरनेट’ और ‘सूचना प्रौद्योगिकी’ सोशल नेटवर्किंग सर्विस के नाम पर ऐसे उत्पाद बना देंगे जो अच्छे खासे आदमी और संस्थाओं की चाल और चरित्र दोनों ही बदल देंगे. जब तक स्मार्ट फोन नहीं थे, तक तक तो काफी हद तक उन कम्प्यूटरों की स्क्रीन के ज़रिए सोशल मीडिया बहुत हद तक दुनिया भर के समाज को सकारात्मकता के साथ जोड़ता रहा जो स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले के बगल में बैठे शख्स को भी नज़र आती थी. ज़्यादातर डेस्कटॉप कम्प्यूटर थे. इन कम्पूटरों के साथ समस्या यह थी कि अक्सर एक आदमी के इस्तेमाल करने के बाद कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को भी पहले वाली गतिविधियां पता चल जाती थीं.
वैसे तो ये लोकतांत्रिक देश में मिले स्वतंत्रता से जीने और अभिव्यक्ति के अधिकार जैसे तोहफों का मामला है, लेकिन प्राइवेसी के नाम पर ऐसे-ऐसे टेक्स्ट और ऑडियो, वीडियो शेयर होने लगे जिनको सार्वजनिक रूप से या ज़िम्मेदारी लेकर साझा नहीं किया जा सकता. उस पर सोशल मीडिया पर नकली आईडी बना कर ‘कुछ भी और कभी भी’ साझा करने के बढ़े चलन ने तो हालात और खतरनाक बनाए. खैर जब तक ये कंटेंट व्यक्ति तक या छोटे से गुट तक सीमित रहे तो इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन जब ये काफी लोगों तक पहुंच जाएं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है.
सोशल मीडिया के इस असर को सबसे ज्यादा और पहले भुनाया प्रचार प्रसार के काम के ज़रिये रोज़ी रोटी चलाने वालों ने. कंटेंट लिखने से लेकर विज्ञापन बनाने वालों ने अपनी विधा से इसका इस्तेमाल उत्पादों को बेचने, बिकवाने के लिए किया. अपनी बात झट से पहुंचाने और फट से फैलाने वाले गुणों वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म (भारत के सन्दर्भ में फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब और इन्स्टाग्राम ख़ास हैं) कितने ही लोगों के लिए मददगार भी साबित हुए और एक बड़ी ज़रूरत बना लिए गए. वहीं , जहां तक मनोरंजन की बात है तो भी इसका इस्तेमाल कुछ हद तक समझ आता है, लेकिन जब कोई चीज़ जीवन के हरेक पहलू को प्रभावित करने लगे तो वो मानवीय चरित्र को भी बदलने लगती है.
भारतीय समाज पर इसके लक्षण अब बहुत साफ़-साफ़ दिखाई देने लगे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म कई व्यवस्थाओं के शानदार विकल्प बनके सामने आए. इस दौरान जबरदस्त तरीके से बढ़े इंटरनेट, आईटी, मोबाइल फोन के चलन के साथ सोशल मीडिया ईलाज करने और करवाने से लेकर, समाज सेवा, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक में मददगार बना. एप्स के तौर पर कई नए उत्पाद आए, जिनके जरिए सरकारी बैठकों से लेकर, वेबिनार, कांफ्रेंस और यहां तक की दुख सुख को साझा करने के कार्यक्रम भी किये गए.
इन सब में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की भी अहम भूमिका रही, चाहे आपसी बातचीत का ऑडियो-वीडियो प्रसारित करना हो या उसकी पूर्व सूचना या रिकार्डेड संस्करण बाद में लोगों तक पहुंचाना हो. कोई शक नहीं कि मानव जाति के लिए खड़े हुए कोरोना के संकटकाल में सोशल मीडिया एक अवतार की तरह भी सामने आया और इसकी लोकप्रियता भी बड़ी. इस दौरान ऐसे बहुत से लोगों को सोशल मीडिया की खूबियां पता चलीं, जिन्होंने पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया. यानि साथ ही इसके उपभोक्ताओं की तादाद भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी. लेकिन इन तमाम खूबियों के कारण ही सोशल मीडिया तरह-तरह के खतरे भी बढ़ाता गया. भारतीय पर्यावरण में तो ये परिलक्षित हो गया है.
दुनियाभर के देशों में भारत सबसे ज्यादा विविधता और विभिन्नताओं वाला देश है. अलग-अलग तरह के खान पान, रहन सहन, पहनावे, परम्पराएं, भाषाएं, बोलियां तो हैं ही, हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में भी यहां की आबादी रहती है. ऐसे में सबकी ज़रूरतें भी अलग-अलग होना स्वाभाविक है. उस पर सैंकड़ों साल की गुलामी का असर, पूजा पाठ के अलग अलग तौर तरीके, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े दलों का होना विचारों में टकराव और मत भेद तो पैदा करेगा ही. अभिव्यक्ति समेत विभिन्न प्रकार की आजादी के मौलिक अधिकारों का मिलना अक्सर इस टकराव को बढ़ावा भी देता है. लोग और विभिन्न संस्थाएं इसका बेजा इस्तेमाल भी करती हैं.
सोशल मीडिया के ज़रिए कही जाने वाली कई बातें और उनकी प्रतिक्रिया ‘अपराध’ के तत्व से भरपूर भी होती हैं, लिहाज़ा ऐसे मामलों में पुलिस या कानून का पालन कराने वाली विभिन्न एजेंसियों की भूमिका सामने आती है. सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर आए दिन पुलिस में केस दर्ज होते हैं. यही नहीं इसमें भी पुलिस एजेंसियों पर पक्षपात या भेदभाव वाला रवैया अख्तियार करने को लेकर विवाद होने लगे हैं. ये सब सामाजिक सद्भाव, भाई चारे और आज़ाद लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. कई अपरिपक्व टीवी चैनलों ने उत्तेजना फैलाकर हालात और बिगाड़े हैं. इसी साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद धार्मिक अवसरों पर हुई घटानाओं की जानकारी समाज में बड़ी कड़वाहट का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया ही है. कर्नाटक, यूपी, पंजाब से लेकर राजधानी दिल्ली समेत कई स्थानों पर इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. ये सिलसिला अब भी चल रहा है. इन हालात ने पुलिस और अदालतों पर भी काम का बोझ बढ़ाया है.
दुनियाभर में सबसे अधिक आबादी वाले देशों की फेहरिस्त में भारत नंबर 2 पर है, लेकिन सोशल मीडिया के मामले में सबसे आगे है. अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के ही अकेले यहां पर 40 करोड़ अकाउंट हैं, वहीं वाट्सऐप के तो तकरीबन 53 करोड़ खाते हैं, जबकि एक अन्य ऐप ट्वीटर के भारत में तकरीबन 23 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हैं. भारत से खूब धन कमा रही इन ऐप्स की विश्वसनियता और अन्य गड़बड़ियों के कारण विवाद भी होते रहते हैं. कई देशों ने तो अपने यहां विभिन्न कारणों से ऐसी ऐप्स पर रोक भी लगा रखी है. गूगल की 2004 में लांच हुई ऑरकुट को लेकर कई केस और विवाद हुए. इस सोशल नेटवर्किंग सर्विस को खुद गूगल ने 10 साल में बंद कर दिया था. भारत समेत कई देशों ने भी बीच-बीच में इन पर रोक लगाई और हटाई है.
ये तो व्यवस्था पर प्रभाव की बात है, लेकिन सोशल मीडिया का असर और भी खतरनाक हालात पैदा कर रहा है. हर उम्र , तबके और पेशे से जुड़ा आम व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सोशल मीडिया के असर में इस कदर आ रहा है कि इसने उसके रहन सहन, खान पान के तरीके से लेकर दूसरों के प्रति सोच तो बदली ही, अपने प्रति भी अजीब तरीके सोचने लगा है. अकेले होने पर ही किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भी पहली फुर्सत में हर शख्स अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए दिखाई दे जाएगा. नहीं तो ईयर फोन या हेड फोन लगाए मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो में आंखें गड़ाए देखा जा सकता है. ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पर चैट करते हुए, टेक्स्ट पढ़ रहे या वीडियो देख रहे मिलेंगे. रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ सुख दुख साझा करने के लिए सामूहिक तौर पर भी मिलेंगे तो वहां भी नज़रें और उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर होंगी.
शादी, समारोह, मेले या कहीं सैर सपाटे पर जाना हो तो ज़्यादातर की पहली प्राथमिकता मोबाइल से तस्वीरें, सेल्फी खींचना होती है. ताकि इस स्थान पर अपनी उपस्थिति को सोशल मीडिया पर दर्ज करा सकें. सोशल मीडिया पर अपनी तरफ ध्यान खींचने की इस कवायद में उस शख्स का उस स्थान पर आने का महत्व ही खत्म हो जाता है. इसका उसे अहसास भी नहीं होता. कुछ तो कार्यक्रमों में आते ही वीआईपी के साथ फोटो या सेल्फी लेने की फिराक में ही रहते हैं. और तो और धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ से लेकर अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर भी लोग बाग सोशल मीडिया के मोहपाश से अलग नहीं हो पाते. कुल मिलाकर ये आदत एक गंभीर खतरनाक नशा बन चुकी है. मां बाप अपने उस उम्र के नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोल कर देने लगे हैं, जिनमें अच्छे-बुरे की तो क्या, अपने बारे में भी ठीक से सोच पाने की ज़हनी ताकत पैदा नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर आने वाला खराब कंटेंट इन बच्चों में स्वाभाविक रूप से उनकी संवेदनाओं को प्रभावित करके विकार भी बढ़ा रहा है.
कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि शो ऑफ़ यानि दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया का असर ऐसे नशे में तब्दील हो रहा है, जिसकी चपेट में फंसते लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है. इस नशे का मज़ा लेने वाला शख्स इसे उन लोगों तक भी पहुंचा देता है, जिनको भले ही उसकी ज़रूरत न हो. कंटेंट शेयर करने वाला ये भी नहीं सोचता कि जो टेक्स्ट या वीडियो वो औरों के साथ साझा कर रहा है, वो सही भी है या नहीं. न ही ज्यादातर लोग उसके पीछे के तर्क का आंकलन कर पाते हैं. लोगों की इसी प्रवृत्ति का फायदा न सिर्फ विज्ञापन बनाने वाले उठाते हैं, बल्कि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा और पूजा पद्धति के विभिन्न तरीकों को धर्म मानने वाले लोग भी उठाते हैं. अब तो अपनी सोच को ही सही और सर्वश्रेष्ठ समझने वाले ऐसे लोगों के समूह अपने हिसाब से कंटेंट बनाने और बनवाने लगे हैं. इसके लिए बाकायदा उन्होंने टीमें बना रखी हैं. अपनी सोच दूसरों के जहन में ठूंसने के लिए लोगों को वेतन और भारी भरकम फीस देकर सेवा में रखा जाता है. यानि लोगों की सोचने समझने की ताकत को प्रदूषित और क्षीण करना ही नहीं इनका मकसद है ताकि अपने हित साधने में वो इसका इस्तेमाल कर सकें.